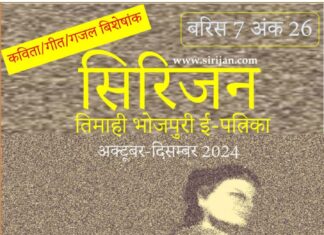संस्कृत में भ्वादिगण के अंतर्गत एगो धातु ह- ‘घ्रा’। धातुसूत्र के अनुसार ‘घ्रा’ सूँघे, पता लगावे के अर्थ में (सकर्मक, अनिट्) बा। घ्राण (घ्रा+क्त) शब्द के जरि में इहे धातु ह जवन सूँघे के क्रिया के अलावे गंध, बास, आ नाक के बोधक ह। ‘आ’ के उपसर्ग के रूप में कुछ शब्दन में लागे से ‘के आरंभ से लेके,’ ‘से,’ ‘से लेके,’ ‘से दूर’, ‘में से’ जइसन बढ़ोतरी भी ओह शब्दन में होला- ‘आ इत्यर्वागर्थे।’ कुछ उदाहरण,
आ+पाद+मस्तक =पैर से लेके सिर तक।
आ+मूल+चूल =जरि से फुनगी तक।
आ+पर्वत =पर्वत से एने।
आ+सेतुसमुद्र =समुद्रसेतु पर्यंत।
आ+घ्राण (आघ्राण) =नाक तक, आदि।
अब हेह ‘नाक तक’ यानि आघ्राण के कवनो अभिधामूलक अर्थ जियादह संगत ना होई, तनी हई बतकही सुनल जाव-
“का पंडितजी, काहे थलबलाइल अस चलत बानीं? कहाँ से आ रहनी हँ?
“भोज से जजमान।”
“अच्छा-अच्छा, फलाना किहाँ से? खूब रहल ह नु?”
“अह्, जनि पूछीं, नाक तक चलल ह। थेईथेई। फलाना बाबू खूब ईजति कइनीं।”
अब बुझाइल होखी आघ्राण के मतलब। ई शब्द भर पेट, भर हीक, तृप्त होखे तक, प्रचूर मात्रा में, ढाला, गलबल (चउपाया पशु के नाद में नाक बुड़ा के खाइल) आदि अर्थ के बोध करावेला। प्राकृत काल में ई शब्द घिस पिट के ‘अग्घाण’ भ गइल। कइसे? देखल जाव-
आ+घ्+र्+आ+ण्+अ =अ+ग्+घ्+आ+ण+अ।
एह परिवर्तन में का भइल बा?
आ के ह्रस्वीकरण, घ् आ र् में से र् व्यंजन के लोप आ अल्पप्राण ग् के आदेश। ‘प्राकृत शब्दानुशासन’ के एगो सूत्र ह- ‘संयोगे’ (प्रा. श. २.४०)। एकर तात्पर्य ई कि संस्कृत से प्राकृत में ध्वनि परिवर्तन में संयोग के पहिले के स्वर ह्रस्व हो जाला, जइसे-
आम्र > अम्ब
ताम्र > तम्ब
शीघ्र > सिग्घं, आदि।
+++
आघ्राण > अग्घाण के अर्थ में कवनो छरन नइखे भइल। तनी विस्तार से-
१- भोजन /पान से तृप्त भइल।
२- संतुष्ट होखल, मन भरल, इच्छा पूरन भइल, परिपूर्ण होखल।
३- प्रसन्न भइल। हरख भरल।
४- थकल, ऊबल।
५- पूर्णता पावल। (आप्टे कोश)
ई सभ अर्थ अजहूँ ले मौजूद बा।
एही आघ्राण भा अग्घाण के क्रियात्मक प्रयोग के शब्द ह- ‘अघा-इल’ (हिं- अघाना), जवन तृप्ति भा पूर्णता पावे के बोधक ह। अग्घाण के अगिला पड़ाव ह – अघा (ना)।
संस्कृत में ‘अन्’ अव्यय निषेधात्मक ‘नञ्’ के स्थानादेश ह आ ई अभाव वा निषेध सूचित करे खाती स्वर से आरंभ होखे वाला शब्दन के पहिले जोड़ल जाला, जइसे- अनन्त, अनधिकार, अनीश्वर। ई कबो-कबो व्यंजन से शुरू होखे वाला शब्दो में सट जाला, जइसे- अनहोनी, अनबन, अनरीति, अनपढ़।
अन् अव्यय के ‘अघा’ में जुड़े से बनल ‘अनघा’। का मतलब होई एकर? ना अघाए भर। ना बुझाइल? चली एगो अउरि उदाहरण देखल जाव-
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ।
[भीष्म से अभिरक्षित हमनी के (सेना के) बल अपर्याप्त बा। भीम से अभिरक्षित उनकर बल पर्याप्त बा।]
अजीब बात। ई कइसे हो सकेला कि लड़े के अगतहीं, उहो अर्जुन जइसन महारथी ई कहे कि हमनी के सेना के बल नाकाफी बा आ ओन्हनि के काफी। दरअसल प्रचूरता सूचक शब्दन के साथ ई बात ध्यान देवे लायक बा। गणित चाहे जेतना होखे ऊ सीमा का भीतर होला बाकी अ+गणित भा अन्+ गणित के सीमा खतम। अंत भी तयशुदा ह बाकी अनंत? पर्याप्त भी सीमा के भीतर ह आ अपर्याप्त? ना स्पष्ट तौर प कम कहल जा सकेला ना ऊपर के कवनो गिनती। अर्जुन बड़बोलापन के बजाय आपन कथनशैली के मर्यादित रखत इहे बात कहले कि भीम से अभिरक्षित हमनी के सेना के बल भी अपरिमित बा।
अब अन्+अघा के बारे में सोचल जाव। ई परितृप्ति भा पूर्णता के दायरा से अतिरेक के बोधक ह- तृप्ति से ऊपर असीमित, पूर्णता से भी जादे।
कुछ एकर रूप धइले अउ शब्द बाड़न जेकर उपस्थिति एह शब्द के लेके भ्रम पैदा करेला, जइसे- ‘अनघ’ =अन्+अघ= पाप रहित।
अनघ/अनध =अनहद/अनाहत- “बाजेला अनघ बधइया हो रामा!”
एन्हनि के मूल आ अर्थ दोसर बा। ध्यान रहे के चाहीं।
✍दिनेश पाण्डेय जी
पटना